
रमेश चौहान एक वरिष्ठ साहित्यकाारहैं, जो हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में समान अधिकार रखते हैं । पद्य में आपका परिचय एक छंदकार के रूप में है तो वहीं गद्य साहित्य में आप एक आलेखकार के रूप में अपना परिचय रखते हैं । सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक विषय पर आपके कलम चलते रहते हैं ।
भारत की लोकसंस्कृति — गीत, नृत्य, रीति-रिवाज और विश्वासों का संगम।
इस साहित्यिक आलेख में हम देखेंगे कि कैसे लोक परंपराएँ, जो हमारे सामूहिक जीवन को आकार देती हैं, हिन्दी साहित्य के विभिन्न कालखंडों में अपनी पहचान बनाए रखती हैं और वर्तमान युग में भी अपनी जड़ों से ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं। यह लोकसंस्कृति भारतीयता की वह अक्षुण्ण धारा है जो साहित्य की हर विधा को प्राण देती है।
लोकसंस्कृति: जीवन की लय और सामूहिक चेतना
भारत की लोकसंस्कृति मात्र परंपराओं का संग्रह नहीं है; यह हमारे सामूहिक जीवन का स्पंदन है—गीत, नृत्य, रीति-रिवाजों और अटूट विश्वासों का वह अनमोल संगम, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह वह जन-संस्कृति है जो शहरों की चकाचौंध से दूर, गाँवों और कस्बों के खेत-खलिहानों, चौपालों और आंगन में साँस लेती है।
लोक परंपराएँ, वास्तव में, हमारे सामाजिक ताने-बाने को आकार देने वाली अदृश्य शक्ति हैं। जन्म के सोहर से लेकर मृत्यु के अनुष्ठानों तक, फसल बोने के गीतों से लेकर ऋतुओं के स्वागत के नृत्यों तक, हर क्रियाकलाप में जीवन की सहजता, श्रम की गरिमा और प्रकृति के साथ मनुष्य के गहरे एकात्म संबंध की अभिव्यक्ति होती है। ये परंपराएँ हमें केवल अतीत से नहीं जोड़तीं, बल्कि वर्तमान में हमें एक समान पहचान और सामूहिक स्मृति प्रदान करती हैं, जो हमें भारतीय होने का बोध कराती है।
साहित्य में लोक का आरोहण
हिन्दी साहित्य, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, इसी लोकसंस्कृति की अक्षुण्ण धारा को अपने भीतर समाहित किए हुए है। साहित्य में लोक की उपस्थिति केवल एक विषय-वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि उस मूल ऊर्जा के रूप में है जो उसकी भाषा, उसके छंद और उसके भावबोध को प्राण देती है।
यह साहित्यिक आलेख इसी गहरे अंतर्संबंध की पड़ताल करता है। हम यह देखेंगे कि कैसे-
- विभिन्न कालखंडों में—भक्तिकाल के संतों की वाणी से लेकर आधुनिक काल के आंचलिक कथाकारों की कलम तक—लोक-जीवन और उसके विश्वासों ने साहित्य की दिशा निर्धारित की।
- बदलते युग और वैश्विकरण की चुनौतियों के बावजूद, लोक परंपराएँ साहित्य के माध्यम से अपनी पहचान को बनाए रखती हैं और समय के साथ खुद को नए संदर्भों में ढालती हैं।
- लोकसंस्कृति, भारतीयता की वह मजबूत नींव है, जो अनेकता में एकता के सूत्र को पिरोती है, और यही कारण है कि यह धारा हिन्दी साहित्य की हर विधा—कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक—को निरंतर ऊर्जावान बनाती रहती है।
यह लोकसंस्कृति हमारी वह जीती-जागती विरासत है, जो साहित्य के दर्पण में सबसे अधिक जीवंत और मुखर दिखाई देती है
विभिन्न कालखंडों में लोकसंस्कृति की उपस्थिति
हिन्दी साहित्य के हर युग ने लोकजीवन और लोकसंस्कृति के तत्वों को भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण किया है:
१. आदिकाल (लगभग १०५० ई. से १३७५ ई.)
इस काल में लोकसंस्कृति का स्वरूप प्रायः वीर गाथाओं, लोकनाट्यों और स्थानीय बोलियों की रचनाओं में मिलता है। आल्हा जैसी वीर गाथाएँ, जो आज भी ग्रामीण अंचलों में सुनाई जाती हैं, लोक-शौर्य, खान-पान और रीति-रिवाजों का चित्रण करती हैं।
- उद्धरण:विद्यापति की पदावली, हालाँकि मुख्य रूप से शृंगार और भक्ति की है, लेकिन उन्होंने जिस भाषा (मैथिली) और लोक-उत्सवों (जैसे बसंत) का प्रयोग किया, वह लोकसंस्कृति की नींव पर खड़ी है।
- स्रोत: विद्यापति की पदावली और नरपति नाल्ह का बीसलदेव रासो जैसे लोक-प्रचलित काव्य।
२. भक्तिकाल (लगभग १३७५ ई. से १७०० ई.)
यह काल लोकसंस्कृति और साहित्य के समन्वय का स्वर्ण युग है। भक्ति आंदोलन का मूल ही लोक-चेतना था। संतों और कवियों ने संस्कृत के पंडितवाद को छोड़कर लोकभाषा (अवधी, ब्रज, सधुक्कड़ी) को अपनाया, जिससे उनका संदेश सीधे जनमानस तक पहुँचा।
- सगुण भक्ति: तुलसीदास ने अवधी को रामकथा का माध्यम बनाकर उत्तर भारत के गृहस्थ धर्म, परिवार और सामाजिक मर्यादाओं को लोक-स्वीकार्य बनाया। सूरदास ने ब्रजभाषा में कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया, जहाँ जन्म, बचपन, होली, और रासलीला जैसे सभी उत्सव लोकजीवन से लिए गए थे।
- निर्गुण भक्ति:कबीर ने अपनी उलटबाँसियों और साखियों में लोक-जीवन के प्रतीकों (जैसे चक्की, जुलाहा, पनघट) और लोक-भाषा को अपनाया।
- उद्धरण: कबीर ने शास्त्रीयता को चुनौती देते हुए जनभाषा का महत्व स्थापित किया:”संस्कृत है कूप-जल, भाखा बहता नीर।”(स्रोत: कबीर ग्रंथावली/लोकप्रचलित कबीर वाणी)
३. रीतिकाल (लगभग १७०० ई. से १९०० ई.)
यह काल दरबारी संस्कृति से प्रेरित था, जहाँ विषय-वस्तु मुख्य रूप से शृंगार थी। फिर भी, रीतिमुक्त कवियों और लोक-रचनाओं में लोकसंस्कृति की झलक मिलती है। शृंगारिक कविताओं में होली, सावन के झूले और ग्रामीण परिवेश से जुड़े उपमानों का प्रयोग हुआ।
वर्तमान कालखंड: जड़ों की ओर लौटना (आधुनिक काल)
आधुनिक काल में, विशेष रूप से २०वीं सदी के मध्य से, लोकसंस्कृति हिन्दी साहित्य के केंद्र में वापस आ गई और साहित्यकारों ने लोकजीवन को केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि स्वयं विषय-वस्तु बना दिया। आधुनिक काल में, विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारतीय लोकसंस्कृति हिन्दी साहित्य के केंद्र में न केवल विषय-वस्तु बनकर लौटी, बल्कि एक सशक्त वैचारिक आधार भी बनी। यह लोक-चेतना अतीत के भावुक स्मरण से कहीं अधिक, पहचान की तलाश और प्रतिरोध की आवाज बनकर उभरी।
क) शुरुआती आधुनिकता और राष्ट्र-प्रेम
भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में, जहाँ एक ओर खड़ी बोली साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर लेखकों ने जानबूझकर लोक-विधाओं और सरल भाषा का प्रयोग किया।
उद्धरण: इस दौर के साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जनता को जागृत करना था, जिसके लिए लोक की भाषा और उसके मुहावरों को अपनाया गया।
जन-जुड़ाव: भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों और प्रहसनों में लोकनाट्य शैली (जैसे नौटंकी, स्वांग) और स्थानीय बोलियों के गीतों का प्रयोग किया ताकि वे जनमानस तक सीधे पहुँच सकें। राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार के संदेश को लोक-शैली के माध्यम से पहुँचाना इस कालखंड की साहित्यिक रणनीति थी।
ख) आंचलिक साहित्य का उदय (The Rise of Regional Literature)
यह वह दौर है जिसने लोकसंस्कृति के जीवंत स्वरूप को सबसे अधिक विस्तार दिया। आंचलिक उपन्यास एक ऐसी विधा बनकर उभरी जिसने किसी विशेष क्षेत्र के गीत, नृत्य, अंधविश्वास, बोली, रीति-रिवाज, और जीवन-संघर्ष को ईमानदारी से प्रस्तुत किया।
- फणीश्वरनाथ ‘रेणु’: इस विधा के जनक माने जाते हैं। उनके उपन्यास ‘मैला आँचल’ ने बिहार के मेरीगंज गाँव के लोकजीवन को अमर कर दिया। इसमें छठ के गीत, होली पर फाग, स्थानीय गालियाँ, टोटके और जन-विश्वासों को इतना प्रामाणिक रूप दिया गया कि साहित्य स्वयं लोक-परंपरा का हिस्सा बन गया।
- उद्धरण (लोक-त्योहारों पर रेणु का चित्रण):“रेणु का आँचलिक उपन्यास मैला आँचल के मेरीगंज गाँव में अनेक पर्व व त्योहार प्रचलित हैं…जिसमें होली के अवसर पर ‘फाग’ लोकगीत गाया जाता है, जो शास्त्रीय संगीत के साथ प्रेम का वर्णन प्रस्तुत करता है।”(स्रोत: ‘लोक साहित्य और हिंदी साहित्य का समन्वय’, बहुविषयक जर्नल से प्राप्त जानकारी)
- नागार्जुन, शिवप्रसाद सिंह और अन्य: नागार्जुन ने अपनी कविताओं में मिथिला के किसान जीवन, अकाल, गरीबी और लोक-विश्वासों को सरल लोक-छंदों में गाया। शिवप्रसाद सिंह के उपन्यासों में भी बनारस और आसपास के ग्रामीण जीवन की गहरी छाप मिलती है।
ग) समकालीन साहित्य में लोकसंस्कृति की प्रासंगिकता
वर्तमान कविता, कहानी और नाटक में लोकसंस्कृति एक नए संदर्भ में उपस्थित है। लेखक अब लोक को केवल नोस्टेल्जिया के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिरोध की चेतना और प्रामाणिक पहचान के स्रोत के रूप में देखते हैं।
- लोक-चेतना और विमर्श: दलित, आदिवासी और स्त्री विमर्श से जुड़े साहित्य में लोकसंस्कृति एक महत्वपूर्ण हथियार है। इन समुदायों की विशिष्ट लोककलाएँ, गीत और परम्पराएँ मुख्यधारा के सामने एक वैकल्पिक और सशक्त जीवन-दृष्टि प्रस्तुत करती हैं।
- नये मिथक और प्रतीक: समकालीन लेखक लोक-कथाओं, मुहावरों और मिथकों का उपयोग आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर टिप्पणी करने के लिए कर रहे हैं। वे लोक-शैली को अपनाकर अपनी अभिव्यक्ति में सरलता और मार्मिकता लाते हैं।
- वैश्विक संदर्भ में पहचान: भूमंडलीकरण के दौर में जब पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, तब भारतीय लोकसंस्कृति (योग, लोक-व्यंजन, परम्परागत कलाएँ) साहित्य के माध्यम से अपनी स्थानीय पहचान को मजबूती से स्थापित कर रही है।
- दार्शनिक आधार: भारतीय संस्कृति का यह लचीलापन और निरंतरता ही उसे जीवंत बनाए रखती है। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है:”कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती, यदि वह अपने को अन्य से पृथक रखने का प्रयास करे।”(स्रोत: भारतीय संस्कृति पर विचार, मूल विचार महात्मा गांधी/अन्य चिंतकों से भी संबंधित, जो सांस्कृतिक समन्वय पर बल देते हैं)यह उद्धरण स्पष्ट करता है कि लोकसंस्कृति ने हमेशा बाह्य प्रभावों को ग्रहण किया, लेकिन साहित्य के माध्यम से अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा।
२१वीं सदी के हिन्दी साहित्य में भारतीय लोकसंस्कृति
२१वीं सदी का हिन्दी साहित्य भूमंडलीकरण, तीव्र तकनीकी प्रगति और विमर्शों की बहुलता के बावजूद, भारतीय लोकसंस्कृति की जड़ों से गहरा जुड़ाव रखता है। इस कालखंड में, लोकसंस्कृति को केवल नोस्टेल्जिया या अतीत के गौरव के रूप में नहीं, बल्कि पहचान, प्रतिरोध और अस्मिता के एक सशक्त माध्यम के रूप में रेखांकित किया गया है।
पहचान और अस्मिता का आधार
२१वीं सदी के साहित्य में लोकसंस्कृति व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान की तलाश का मुख्य आधार बनी है।
- आदिवासी और दलित विमर्श: इस काल में आदिवासी और दलित साहित्य ने अपनी विशिष्ट लोकसंस्कृति, मौखिक इतिहास, अनुष्ठान और लोक-देवताओं को केंद्रीय स्थान दिया है। यह लोक-चेतना उनके लिए अस्मिता की घोषणा है, जो सदियों से उपेक्षित रहे हैं। उदाहरण के लिए, आदिवासी लेखकों ने अपनी पारंपरिक कलाओं, जैसे सोहराई चित्रकला या सरहुल नृत्य की सांस्कृतिक महत्ता को अपने लेखन में उतारा है।
- स्त्री और लोकगीत: समकालीन स्त्री लेखिकाओं ने लोकगीतों और महिलाओं के पारंपरिक रीति-रिवाजों (जैसे विवाह गीत, तीज-त्योहार) का विश्लेषण पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझने और चुनौती देने के लिए किया है। ये गीत जहाँ एक ओर स्त्रियों के दुःख और दमित इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सामूहिक संघर्ष और प्रतिरोध की नींव भी बनते हैं।
बदलते संदर्भों में लोक का लचीलापन
२१वीं सदी का साहित्य लोकसंस्कृति के जीवंत स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें वह आधुनिकता के साथ संवाद स्थापित करती है।
- शहरी लोक और ग्लोबल गाँव: लेखक अब केवल ग्रामीण लोक पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, बल्कि शहरी लोक (Urban Folk) और प्रवासी भारतीयों की लोकसंस्कृति को भी दर्शा रहे हैं। भूमंडलीकरण के दबाव में भी, लोग छोटे-छोटे सांस्कृतिक द्वीप (Cultural Enclaves) बनाकर अपनी लोक परंपराओं—जैसे क्षेत्रीय व्यंजन, भाषा के मुहावरे और पर्वों—को जीवित रखे हुए हैं।
- टेक्नोलॉजी और लोककला: साहित्य में इस बात का चित्रण बढ़ा है कि कैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लोककलाओं (जैसे लोक संगीत, लोकनृत्य) और लोककथाओं के प्रसार के लिए नए मंच प्रदान किए हैं, जिससे लोक का स्वरूप डिजिटल और व्यापक हो गया है।
प्रतिरोध और सामाजिक न्याय की आवाज
लोकसंस्कृति अब केवल सुंदर परंपरा नहीं रही, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रतिरोध की एक शक्तिशाली रणनीति बन गई है।
- लोक-कथाओं का पुनर्कथन: समकालीन कथाकार और कवि पुराने लोक-मिथकों और लोक-कथाओं को आज के संदर्भ में पुनर्कथित (Re-tell) कर रहे हैं। इन कहानियों का उपयोग वे राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और पर्यावरण विनाश जैसे ज्वलंत मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए कर रहे हैं।
- लोक की भाषा और विद्रूप: कई लेखकों ने लोक की सरल, सीधी और व्यंग्यात्मक भाषा शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं में विद्रूप (Irony) और तीखापन पैदा किया है। यह लोक की भाषा ही है जो व्यवस्था के दोगलेपन को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उजागर करती है।
उपसंहार
हिन्दी साहित्य में भारतीय लोकसंस्कृति की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। गीत, नृत्य, रीति-रिवाजों और विश्वासों का यह संगम एक जीवंत ऊर्जा है, जो हर कालखंड में साहित्य को प्रेरित करता रहा है। वर्तमान कालखंड में, आंचलिक साहित्य से लेकर समकालीन विमर्शों तक, लोकसंस्कृति न केवल भारत के सामूहिक जीवन को आकार दे रही है, बल्कि आधुनिकता की चुनौतियों के बीच हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह वह धरोहर है, जिसे साहित्य ने सँजोकर, उसे अमर बना दिया है।
२१वीं सदी का हिन्दी साहित्य भारतीय लोकसंस्कृति को जड़ों की ओर लौटने के एक अनिवार्य माध्यम के रूप में देखता है। यह लोकसंस्कृति भारतीयता की अक्षुण्ण धारा है, जो न केवल हमारे अतीत को सँजोती है, बल्कि वर्तमान के जटिल विमर्शों को एक प्रामाणिक आधार और भविष्य के लिए प्रतिरोध की ऊर्जा भी प्रदान करती है।

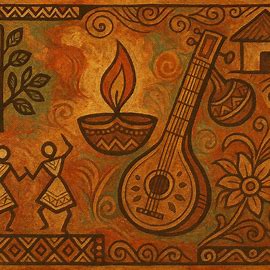




Leave a Reply