
प्रस्तावना: साहित्य – जीवन का शाश्वत संवाद
साहित्य, मानव सभ्यता के साथ विकसित हुआ एक शाश्वत संवाद है। इसे प्रायः “समाज का दर्पण” कहा जाता है, क्योंकि यह अपने समय की परिस्थितियों, मान्यताओं, संघर्षों और संवेदनाओं को यथार्थवादी ढंग से प्रतिबिंबित करता है। महान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा था, “किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता कि चित्तवृत्तियों का संचित फल होता है।” (स्रोत: हिंदी साहित्य का इतिहास) यह कथन साहित्य की परावर्तक भूमिका को स्पष्ट करता है।
किंतु, साहित्य की भूमिका केवल परावर्तन तक सीमित नहीं है; यह उससे कहीं अधिक सक्रिय और गतिशील है। बदलती हुई दुनिया में—जहाँ मूल्य, तकनीक और राजनीति निरंतर परिवर्तनशील हैं—साहित्य केवल अतीत को दर्ज नहीं करता, बल्कि वर्तमान को चुनौती देता है और भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। इसलिए, यह कथन पूर्णतः सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, दिशा-सूचक भी है।
साहित्य और समाज : परस्पर प्रतिबिंब
साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है, पर यह दर्पण केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता, वह प्रश्न भी करता है। समाज बदलता है — उसके मूल्य, उसकी सोच, उसकी गति — और साहित्य उस परिवर्तन को दिशा देता है।
आज जब जीवन की रफ़्तार तेज़ है, संबंधों की परिभाषाएँ बदल रही हैं, तब लेखक का कलम नई संवेदनाओं की खोज में है। आधुनिक लेखन अब केवल कथा या कविता नहीं रहा, यह अनुभवों का साझा मंच बन गया है।
साहित्य की दोहरी भूमिका: दर्पण और दिशा-सूचक
साहित्य दो महत्वपूर्ण कार्यों को एक साथ संचालित करता है:
1. दर्पण: यथार्थ का प्रतिबिंबन
साहित्य अतीत और वर्तमान की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं को निष्पक्ष रूप से दिखाता है। यह समाज की विसंगतियों, अच्छाइयों, बुराइयों, संघर्षों और उत्सवों को दर्ज करता है।
- मूल्यों का चित्रण: प्रेमचंद का साहित्य, विशेषकर ‘गोदान’ (स्रोत: उपन्यास ‘गोदान’), भारतीय कृषक समाज की साहूकारी शोषण, गरीबी और आदर्शों के टूटने के यथार्थ को दर्शाता है। यह उस युग के ग्रामीण जीवन और नैतिक मूल्यों का सच्चा दर्पण है।
- ऐतिहासिक परिस्थितियों का अंकन: भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएँ ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज की पराधीनता, कुरीतियों (जैसे बाल-विवाह, सती प्रथा) और नव-जागरण की शुरुआती चेतना का सटीक चित्रण करती हैं। (स्रोत: भारतेंदु ग्रंथावली)
2. दिशा-सूचक: क्रांति का उद्घोष
साहित्य केवल चित्रण नहीं करता, बल्कि समीक्षा करता है, सवाल उठाता है और परिवर्तन की राह दिखाता है। यह पाठकों को विचार करने, विद्रोह करने और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है।
- राष्ट्रीय चेतना का प्रसार: बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास ‘आनंदमठ’ (स्रोत: उपन्यास ‘आनंदमठ’) ने ‘वंदे मातरम्’ जैसे गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व जोश और दिशा प्रदान की। यह केवल तत्कालीन विद्रोह का चित्रण नहीं था, बल्कि भविष्य के स्वतंत्र राष्ट्र की ओर इंगित करने वाला एक मार्गदर्शक था।
- सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार: कबीर और अन्य भक्तिकाल के कवियों ने अपनी साखियों और पदों (स्रोत: कबीर ग्रंथावली) के माध्यम से जातिवाद, आडंबर और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण पर सीधे प्रहार किया, जो सदियों बाद भी सामाजिक समानता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।
लेखन की नई प्रवृत्तियाँ
डिजिटल युग में साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है। ब्लॉग, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म — ये सब अब रचनात्मकता के नए माध्यम हैं।
युवा लेखक अब अपने विचारों को केवल छापे हुए शब्दों तक सीमित नहीं रखते, वे आवाज़, दृश्य और अनुभवों के माध्यम से नई अभिव्यक्ति खोज रहे हैं। यह बदलाव साहित्य को अधिक लोकतांत्रिक बना रहा है — जहाँ हर आवाज़ को सुनने का अवसर मिल रहा है।
भाषा की जीवंतता
भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, वह संस्कृति की आत्मा है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बंगला, तमिल, या किसी भी भारतीय भाषा में लिखा साहित्य अपने समाज की नब्ज़ बताता है।
आज की चुनौती है — भाषा को जीवित, प्रासंगिक और आकर्षक बनाए रखना। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमें साहित्य को उनकी जीवनशैली से जोड़ना होगा, ताकि भाषा केवल किताबों में नहीं, दिलों में बस सके।
बदलते मूल्यों के बीच साहित्य की प्रासंगिकता
मूल्य किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं। आधुनिकता और वैश्वीकरण के दौर में पारंपरिक मूल्यों में गिरावट आई है, और भौतिकवाद तथा व्यक्तिवाद प्रमुख हो गए हैं।
मानवीय मूल्यों का संरक्षण और पुनर्स्थापना
बदलते समाज में साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानवता को बचाना है।
- विवेक और सहिष्णुता: साहित्य विवेक, करुणा और मानवीयता के सार्वभौमिक मूल्यों को पुनर्जीवित करता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के साहित्य (जैसे अल्बेयर कामू की रचनाएँ) ने अस्तित्ववाद के माध्यम से मनुष्य के अकेलेपन और स्वतंत्रता पर विमर्श खड़ा किया, जिससे पाठकों को जीवन का अर्थ खोजने की नई दिशा मिली। (स्रोत: ‘द प्लेग’, अल्बेयर कामू) । ओमप्रकाश वाल्मीकि की जूठन (आत्मकथा) जहां एक दलित परिवार-अनुभव का मार्मिक जीवन-वृतांत — उपछेद, अपमान और सामाजिक बहिष्कार के जीवंत किस्से हैं। यह अवहेलित वास्तविकताओं को सामने लाकर सामाजिक सहिष्णुता, समानता और मानवता पर विमर्श तेज किया — सीधे-सीधे समावेशन के सिद्धांत को साहित्य से सक्रिय किया। इसी प्रकार कई उदाहरण हैं ।
- विविधता का सम्मान: समकालीन साहित्य हाशिये के समाज (दलित, स्त्री, आदिवासी) के अनुभवों को सामने लाकर समावेशी मूल्यों को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में संवेदनशीलता और बहुलता के प्रति सम्मान बढ़ता है। महाश्वेता देवी — Hajar Churashir Maa / Mother of 1084 (बंगाली, 1974) नक्सलवादी युग की पृष्ठभूमि में एक माँ की त्रासदी — हाशिये के राजनीतिक संघर्षों और राज्य-हिंसा का पक्ष-दर्शनीय चित्रण। शोषित वर्गों के राजनीतिक दर्द और सामाजिक अन्याय को साहित्य के माध्यम से उजागर कर यह कृति संवेदनशीलता और न्यायपरक सोच को बढ़ाती है।
तकनीक के प्रभाव में साहित्य का रूपांतरण
तकनीकी क्रांति, विशेषकर डिजिटल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ने साहित्य के स्वरूप और प्रसार को बदल दिया है।
1. विधा और माध्यम का विस्तार
साहित्य अब केवल किताबों तक सीमित नहीं है।
- डिजिटल और हाइपरटेक्स्ट कथाएँ: साहित्य अब ई-बुक्स, ऑडियोबुक्स, पॉडकास्ट और हाइपरटेक्स्ट फिक्शन (नॉन-लीनियर कथाएँ) के रूप में भी उपलब्ध है। यह नए माध्यमों का उपयोग करके युवा पाठकों तक पहुँच रहा है और कथा कहने के नए तरीके खोज रहा है।
- व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया: ब्लॉगिंग और माइक्रो-फिक्शन ने प्रत्येक व्यक्ति को लेखक बना दिया है। यह आम आदमी की समस्याओं और विचारों को तुरंत सार्वजनिक मंच पर लाकर समाज में त्वरित चेतना के प्रसार का कार्य कर रहा है।
2. तकनीक की आलोचना और चेतावनी
साहित्य तकनीकी विकास के खतरों के प्रति भी आगाह करता है।
- साइबरपंक (Cyberpunk) फिक्शन: यह विधा (जैसे विलियम गिब्सन की रचनाएँ) भविष्य के उन समाजों का चित्रण करती है जहाँ तकनीक हावी है और मानवीय नैतिकता खतरे में है। यह समाज को आगाह करता है कि तकनीक का अमानवीय उपयोग विनाशकारी हो सकता है। (स्रोत: ‘न्यूरोमैंसर’, विलियम गिब्सन)
बदलती राजनीति और साहित्य का हस्तक्षेप
राजनीति का सीधा संबंध सत्ता और शक्ति संरचना से होता है। साहित्य, शक्ति के अंधाधुंध उपयोग पर लगातार प्रश्नचिह्न लगाता है।
1. प्रतिरोध और विपक्ष का स्वर
लोकतंत्र के विकास के साथ जब राजनीति ने अपने कई रंग बदले, तब साहित्य ने केवल दर्पण का काम नहीं किया, बल्कि वह दिशा-सूचक भी बन गया। जब सत्ता का स्वर एकमुखी होने लगा, तब लेखकों ने समाज के अंतरात्मा की आवाज़ बनकर प्रश्न उठाए। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य, श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी, और मन्नू भंडारी के महाभोज जैसे साहित्यिक हस्तक्षेपों ने यह स्पष्ट किया कि साहित्य केवल सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का प्रहरी है। इन कृतियों ने सत्ता के अहंकार, भ्रष्टाचार और जनविमुखता पर करारी चोट की, यह दर्शाते हुए कि जब संस्थाएँ मौन हो जाएँ, तब कलम बोलती है।
नागार्जुन और केदारनाथ सिंह की कविताओं से लेकर शमशेर बहादुर सिंह के संवेदनशील लेखन तक — हर दिशा में साहित्य ने विवेक, संवेदना और प्रतिरोध का स्वर जीवित रखा। यह वही स्वर है जो जॉर्ज ऑरवेल के 1984 या मंटो की विभाजन-आधारित कहानियों में दिखाई देता है — जहाँ लेखक सत्ता से नहीं, सत्य से निष्ठा निभाता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य ने यह सिद्ध किया कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति केवल कलात्मक नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है; और यही साहित्य का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक योगदान है।
साहित्य लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाता है।
- तानाशाही का विरोध: जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास ‘उन्नीस सौ चौरासी’ (1984) (स्रोत: उपन्यास ‘1984’) सर्वसत्तावादी शासन (Totalitarianism) के खतरों का एक शाश्वत साहित्यिक उदाहरण है। यह आज भी सरकारी निगरानी, सत्य के विरूपण (Post-Truth) और स्वतंत्रता के हनन जैसे राजनीतिक मुद्दों की प्रासंगिकता को दर्शाता है। यह केवल तत्कालीन राजनीति का दर्पण नहीं था, बल्कि भविष्य के राजनीतिक खतरों के प्रति एक स्पष्ट दिशा-निर्देश था।
- युद्ध और विस्थापन की त्रासदी: सआदत हसन मंटो की कहानियाँ (स्रोत: मंटो की कहानियाँ) भारत-पाकिस्तान विभाजन की राजनीतिक त्रासदी और उसके मानवीय प्रभाव को बेबाकी से दर्शाती हैं। यह राजनीतिक निर्णयों के मानवीय परिणाम को सामने लाती हैं और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं।
2. राजनीतिक विचारधाराओं का विमर्श
साहित्य राजनीतिक चेतना को केवल जगाता नहीं, उसे परिपक्व और मानवीय दिशा भी देता है। जब राजनीति ध्रुवीकरण और सत्ता-संरक्षण के दायरे में सीमित होती है, तब साहित्य जनता को विवेक और संवाद की राह दिखाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कवि दिनकर, मुक्तिबोध और नागभूषण पटनायक जैसे रचनाकारों ने यह भूमिका निभाई। दिनकर की रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा जैसी कृतियाँ नायकत्व, नीति और संघर्ष के माध्यम से यह स्पष्ट करती हैं कि सच्चा नेतृत्व अन्याय के प्रतिकार में जन्म लेता है — सत्ता की गोद में नहीं।
प्रगतिशील लेखन आंदोलन (1940–70) और नई कहानी आंदोलन (मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर) ने समाजवादी और मानवतावादी विचारधाराओं के बीच पुल बनाया। मुक्तिबोध की अंधेरे में एक दार्शनिक आत्म-संघर्ष है — जहाँ कवि स्वयं से पूछता है कि “क्या मैं सचमुच जनता के साथ हूँ?” यह प्रश्न आज भी राजनीति के हर युग में प्रासंगिक है। वहीं मन्नू भंडारी और भीष्म साहनी के लेखन ने जनमानस और सत्ता के बीच खड़ी नैतिक दीवार को तोड़ा। भीष्म साहनी का तमस राजनीति की विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर गहरा प्रहार है — वह बताता है कि विचारधारा जब संवेदना से कट जाती है, तो हिंसा और अंधविश्वास जन्म लेते हैं।
इस प्रकार, बदलते समाज में साहित्य विचारधारा का विरोध नहीं, बल्कि उसका आत्म-मूल्यांकन कराता है। वह बताता है कि राजनीति यदि सत्ता की भाषा है, तो साहित्य उसकी आत्मा की आवाज़ — जो हमें याद दिलाती है कि किसी भी विचार की कसौटी अंततः मानवता ही होती है।
साहित्य की निरंतर प्रासंगिकता
तेज़ी से बदलती दुनिया — जहाँ तकनीक हमारे सोचने का ढंग तय कर रही है, राजनीति हमारी प्राथमिकताएँ बाँट रही है, और मूल्य लगातार रूप बदल रहे हैं — वहाँ साहित्य अब भी मानवता का सबसे स्थायी आधार है। वह न तो काल से बंधता है, न विचारधाराओं से; क्योंकि उसका केंद्र मनुष्य है — उसकी संवेदना, उसकी कल्पना और उसकी संस्कृति।
संवेदना और सहानुभूति साहित्य की पहली पहचान है। तकनीक हमें सूचना देती है, राजनीति हमें दिशा देती है, पर साहित्य हमें मनुष्य बने रहना सिखाता है। प्रेमचंद की कहानियों से लेकर निर्मल वर्मा की संवेदनशील गद्य-शैली तक, साहित्य ने हमेशा “दूसरे के दुःख को अपना दुःख” बनाने की कला सिखाई। यही सहानुभूति किसी भी सभ्य समाज की आत्मा है — वह पुल जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है।
कल्पना और सृजन साहित्य का दूसरा स्थायी आयाम है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मानव मन की विकास-यात्रा को कल्पना के प्रतीकों में रूपांतरित किया, वैसे ही समकालीन विज्ञान कथा (जैसे जे.सी. भगत की बीसवीं सदी के रोबोट या हिंदी विज्ञान-कथाकार हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचनाएँ) ने भविष्य की संभावनाओं पर विचार कराया। साहित्य न केवल जो है, उसे दिखाता है — बल्कि जो हो सकता है, उसकी कल्पना भी करता है।
भाषा और संस्कृति का वाहक होने के कारण साहित्य हमारी जड़ों को सींचता है। जब नई पीढ़ियाँ डिजिटल शब्दावली में उलझ जाती हैं, तब कवि और लेखक उन्हें अपनी भाषा की आत्मा से जोड़ते हैं। मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, और विनोद कुमार शुक्ल जैसे रचनाकारों ने हिंदी को जीवंत, आधुनिक और आत्मीय बनाए रखा। इसी प्रकार क्षेत्रीय साहित्य — चाहे वह चंद्रकांत देवताले की बस्तर-केन्द्रित कविताएँ हों या हबीब तनवीर के नाट्य रूपांतरण — हमारी सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखते हैं।
इसलिए, बदलते समय में भी साहित्य केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की नैतिक दिशा है। जब सभ्यता शोर में डूबती है, तब साहित्य ही वह मौन स्वर है जो मनुष्य को उसके भीतर के मनुष्य से मिलाता है।
निष्कर्ष: साहित्य ही भविष्य की नींव है
साहित्य की भूमिका सदैव केवल समाज के वर्तमान को चित्रित करने तक सीमित नहीं रही; उसने हर युग में भविष्य के मार्ग को आलोकित करने का कार्य भी किया है। यह मात्र एक दर्पण नहीं, जो हमें यह दिखाए कि हम कौन हैं — बल्कि एक प्रकाश-मशाल है, जो यह बताती है कि हम क्या बन सकते हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
बदलते मूल्यों और निरंतर परिवर्तित होती सभ्यता के बीच साहित्य मानवीयता का संरक्षक है। तकनीक के युग में यह विवेक और संवेदना का आह्वान करता है, और राजनीतिक उथल-पुथल के समय यह न्याय, प्रतिरोध और संवाद का स्वर बनकर उभरता है। वह सत्ता से नहीं, सत्य से निष्ठा रखता है — और यही उसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है।
जब तक मनुष्य अपने भीतर प्रश्न, पीड़ा और स्वप्न महसूस करता रहेगा, तब तक साहित्य जीवित रहेगा — उसके साथ चलते हुए, उसे दिशा देते हुए। वह हर युग से कहता रहेगा:
“मैं तुम्हारा इतिहास भी हूँ और तुम्हारा भविष्य भी।”
इसलिए, साहित्य केवल बीते समय की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है — वह चेतना जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है।
-रमेश चौहान
संपादक, सुरता:साहित्य की धरोहर



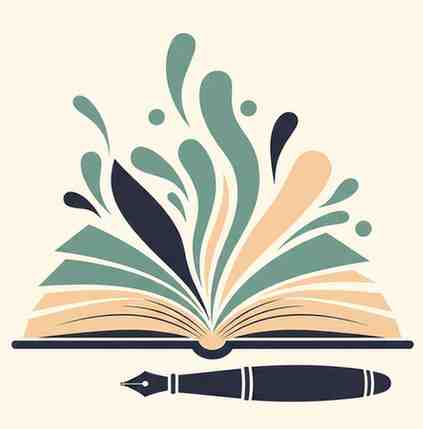

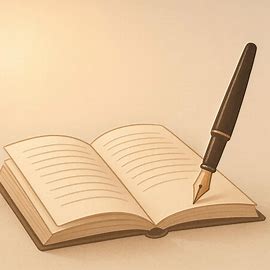
Leave a Reply