हिन्दी साहित्य में क्षेत्रीय बोली-भाषाओं का योगदान
-रमेश चौहान

हिन्दी साहित्य को संपन्न बनाने क्षेत्रीय बोली-भाषाओं की भूमिका-
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार -‘साहित्य जनता की चित्त-वृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब अर्थात समाज का दर्पण है।‘ जब साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज के सभी आयामों का प्रतिबिम्ब दर्पण में अंकित होंगी ही । जब हम भारतीय समाज के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, तो भारतीय विविधता स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होने लगते हैं । इन्ही विविधता में भाषायिक विविधता सम्मिलित है । भाषायी विविधता के संदर्भ में कहा गया है -‘‘‘चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी‘‘ एवं इसी संदर्भ में कबीरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है – ‘‘संस्कृति है कूप जल, भाखा बहता नीर।‘‘ इससे अनुमान लगाया जा सकता है हमारे देश में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। जिनका दर्पण रूपी साहित्य में प्रतिबिम्ब अंकित होना अवश्यसंभावी है । किन्तु आचार्य संजीव ‘सलील‘ मानते है -‘‘साहित्य जड़वत दर्पण नही है अपितु यह सजीव प्रतिक्रियात्मक है जो समाज को सचेत भी करता है।‘ साहित्य के प्रतिक्रियात्मक चेतना के बल पर बोली सवंर्धित-प्रवर्धित होकर साहित्य में स्थान बनाती है। साहित्य किसी भाषा का लैखिक एवं मौखिक स्वरूप का सम्मिश्रण होता है । मौखिक रूप से बोली जाने वाली भाषा लोगो के मौलिक मातृबोली से प्रभावित होती है। अतः स्पष्ट है कि-साहित्य को संपन्न बनाने में इन बोलियों की विशेष भूमिका होती है ।
भाषा-बोली का विकास –
जब हम हिन्दी साहित्य में क्षेत्रीय बोलियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें भाषा के विकास क्रम पर चिंतन करना चाहिये । हिन्दी का विकास क्रम-संस्कृत→ पालि→ प्राकृत→ अपभ्रंश→ अवहट्ट→ प्राचीन → प्रारम्भिक हिन्दी मानी जाती है । अपभ्रंष से हिन्दी उदगम पथ पर क्षेत्र विशेष के प्रभाव से विभिन्न शैलियों का जन्म हुआ विस्तृत क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ उसे हिन्दी एवं सीमित क्षेत्र में विकसित शैलियों को बोलियां कहा गया । अपने रहन-सहन, प्राकतिक वातावरण के अनुरूप विभिन्न भाषा-बोली का विकास हुआ है।
हिन्दी साहित्य का विकास –
हिन्दी साहित्य का विकास आठवीं शताब्दी से माना जाता है । हांलाकि इसकी जड़े प्राचाीन भारत के प्राचीन ‘संस्कृत‘ भाषा में तलाशी जा सकती है । किंतु हिन्दी साहित्य की जड़े मध्ययुगीन भारत के छोटे-छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों में पाई जाती हैं । मध्यकाल में ही हिन्दी का स्वरूप स्पष्ट हुआ तथा उसकी प्रमुख बोलियाँ विकसित हुई । हिन्दी के मुख्य दो भेद पूर्वी हिन्दी एवं पश्चिमी हिन्दी स्वीकार किये गये हैं । पूर्वी हिन्दी के अंतर्गत अर्धमागधी प्राकृत स्वभाव के अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को रखा गया है। पश्चिमी हिन्दी के अंतर्गत पांच बोलियां -खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, और बुंदेली स्वीकार किये गये हैं । इनके अतिरिक्त बिहारी, राजस्थानी एवं पहाड़ी हिन्द प्रदेश की उपभाषएं (बोलियां) स्वीकार की गई हैं । गैर हिन्दी भाषीय क्षेत्र में बोली जानी वाली हिन्दी बोली में – बम्बईया हिन्दी, कलकतिया हिन्दी एवं दक्खिनी हिन्दी भी सम्मिलित है । श्री मधूधवन ने अपनी पुस्तक ‘हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास‘ में भूमिका देते हुये स्वीकार करते हैं कि -‘ इन सभी भाषाओं के साहित्य को हिन्दी का साहित्य माना जाता है क्योंकि ये भाषाएँ हिन्दी साहित्य के इतिहास में ‘अपभ्रंश’ काल से उन समस्त रचनाओं का अध्ययन किया जाता है उपर्युक्त उपभाषाओं में से भी लिखी हो।‘‘ वास्तव में ‘हिन्दी‘ शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिन्दी जिस भाषा समूह का नाम है, उसमें आज के हिंदी प्रदेश/क्षेत्र की 5 उपभाषाएँ तथा 17 बोलियाँ शामिल हैं। वस्तुतः इन बोलियों या उपभाषाओं को हिन्दी भाषा की बोली या उप भाषा मानने के पीछे इन सबकी परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनितिक एकता के साथ-साथ परस्पर बोधगम्यता, शब्द-वर्ग की समानता तथा संरचनात्मक साम्य है ।
हिन्दी की विविधता उसकी शक्ति है –
हिन्दी की विविधता उसकी शक्ति है । हिन्दी की बोलियां अपने साथ एक बड़ी परंपरा एवं सभ्यता को समेटे हुये हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है । हिन्दी साहित्य के जिस कालखण्ड़ को ‘स्वर्ण युग‘ की संज्ञा दी गई, उस काल पर दृश्टिपात करने से हम पाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ‘अवधी‘ में रचित ‘रामचरित मानस‘, सूरदासजी द्वारा ‘ब्रजभाषा‘ में रचित ‘सूरसागर‘ मीरा बाई का राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में साहित्यिक उपादान ‘बरसी का मायरा‘ एवं ‘गीत गोंविंद टीका‘, विद्यापति के मैथली की रचनाएं आदि आज हमारी साहित्यिक धरोहर हैं।
भिन्न बोलियों एवं उपभाषाओं का हिन्दी साहित्य में प्रभाव-
विभिन्न बोलियों एवं उपभाषाओं का हिन्दी साहित्य में आदिकाल से आज पर्यंत सतत प्रभाव बना हुआ है –
अवधी-
अवधी अपने आदिकाल से ही हिन्दी की प्रमुख उप भाषा के रूप में रही है । हिन्दी साहित्य अवधी साहित्य पर निर्भर रहा है । अवधी की पहली कृति मुल्ला दाउद की ‘चंद्रायन‘ या ‘लोरकहा‘ (1370 ई.) मानी जाती है। इसके उपरान्त अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफीध्प्रेममार्गी कवियों को है। कुतबन (मृगावती), जायसी (पद्मावत), मंझन (मधुमालती), आलम (माधवानल कामकंदला), उसमान (चित्रावली), नूर मुहम्मद (इन्द्रावती), कासिमशाह (हंस जवाहिर), शेख निसार (यूसुफ जुलेखा), अलीशाह (प्रेम चिंगारी) आदि सूफी कवियों ने अवधी को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। बैसवाड़ी अवधी में गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा रचित ‘रामचरित मानस‘ ने हिन्दी साहित्य को नई ऊंचाई पर पहुॅचाया । ‘रामचरित मानस‘ के रूप में आज भी हिन्दी साहित्य के रूप में घर-घर स्थापित है ।
ब्रजभाषा-
हिंदी साहित्य के मध्ययुग में ब्रजभाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ। इसलिए इसे बोली न कहकर आदरपूर्वक भाषा कहा गया। मध्यकाल में यह बोली संपूर्ण हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य हो गई थी। पर साहित्यिक ब्रजभाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों के शब्दों और प्रयोगों को भी ग्रहण किया है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का ‘प्रद्युम्न चरित‘(1354 ई.) है। भक्तिकाल में कृष्णभक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रजभाषा का चरम विकास किया। पुष्टि मार्ग-शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय के सूरदास (सूरसागर), नंददास, निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य सम्प्रदाय के गदाधर भट्ट, राधावल्लभ सम्प्रदाय के हित हरिवंश एवं सम्प्रदाय निरपेक्ष कवियों में रसखान, मीराबाई आदि प्रमुख कृष्णभक्त कवियों ने ब्रजभाषा के साहित्यिक विकास में अमूल्य योगदान दिया । इन भक्तों के पद आज भी पूरे हिन्दी भाशाी प्रदेषों में प्रचलित हैं ।
खड़ी बोली-
इसी बोली के आधार पर हिन्दी का आधुनिक रूप खड़ा हुआ है । प्राचीन हिन्दी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरम्भिक प्रयोगों से उसके आदि रूप या बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरहपा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं में उपलब्ध है। इन रचनाकारों में हमें अपभ्रंश-अवहट्ट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्टतः दिखाई देती है। श्रीधर पाठक की प्रसिद्व रचनाएं एकांत योगी और कश्मीर सुषमा खड़ी बोली की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामनरेश द्विवेदी ने अपने पथिक मिलन और स्वप्न महाकाव्यों में इस बोली का विकास किया। अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध‘ के ‘प्रिय प्रवास‘ को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया है।
दक्खिनी-
हिन्दी में गद्य रचना परम्परा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिन्दी के रचनाकारों को ही है। दक्कनी हिन्दी को उत्तर भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी (1688-1741) को है। वह मुगल शासक मुहम्मद शाह ‘रंगीला‘ के शासन काल में दिल्ली पहुँचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिन्दी को लोकप्रिय बनाया। डाॅं कुंज मेत्तर के अनुसार आधुनिक खड़ीबोली हिन्दी का विकास दक्षिण के हिन्दीतर क्षेत्रों में हुआ वे लिखते हैं -‘‘हिन्दी का जो रूप हमारे सामने है उसका पूववर्ती रूप दक्षिण में विकसित हुआ । खड़ी बोली के दक्षिण में व्यवहृत पुराने स्वरूप को देखकर हम यह विष्वास करने को बाध्य हो जाते है कि भाशा की दृश्टि से आधुनिकता के तत्व आरंभकालिन दक्खिनी में अभिव्यक्त हुये थे ।‘‘
छत्तीसगढी-
छत्तीसगढी के प्रांरभिक लिखित रूप के बारे में कहा जाता है कि वह 1703 ईस्वी के दंतेवाडा के दंतेश्वरी मंदिर के मैथिल पंडित भगवान मिश्र द्वारा शिलालेख में है । कबीर दास के शिष्य और उनके समकालीन (संवत 1520) धनी धर्मदास को छत्तीसगढ़ी के आदि कवि का दर्जा प्राप्त है, जिनके पदों को आज भी कबीर अनुनायियों द्वारा गाया एवं पढ़ा जाता है । हिन्दी साहित्य में माधवराव सप्रे के जिस कहानी ‘टोकरी भर मिट्टी‘ को प्रथम सुगठित कहानी होने को श्रेय प्राप्त है, उसकी पृष्ठ छत्तीसगढ़ी लोकगाथा में अवलंबित है । पं. सुन्दरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडेय, मुकुटधर पांडेय, नरसिंह दास वैष्णव, बंशीधर पांडेय, शुकलाल पांडेय, कुंजबिहारी चैबे, गिरिवरदास वैष्णव ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौर में अपनी रचनाओं द्वारा छत्तीसगढ़ी के उत्कर्ष को नया आयाम दिया ।
बुंदेली –
हिंदी साहित्य के विकास और समृद्धि में लोक भाषा बुंदेली का महत्वपूर्ण योगदान है। इसे किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं आंका जा सकता है। इसका विकास रासो काव्य धारा के माध्यम से हुआ। जगनिक आल्हाखंड तथा परमाल रासो प्रौढ़ भाषा की रचनाएं हैं। बुंदेली के आदि कवि के रुप में प्राप्त सामग्री के आधार पर जगनिक एवं विष्णुदास सर्वमान्य हैं, जो बुंदेली की समस्त विशेषताओं से मंडित हैं।
सभी बोलियों ने हिन्दी को आधार दिया है-
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय सभी प्रदेश अंचल राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हुये, जिससे सभी बोलियों में राष्ट्रीयता का नाद गुंजा जिससे हिन्दी साहित्य आज भी गुजिंत है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मौखिक रूप से हिन्दी-उर्दू-क्षेत्रीय बोलियों से मिश्रित हिन्दी का उपयोग किया गया जिसे हिन्दूस्तानी के नाम से गांधी आदि नेताओं द्वारा अभिहित किया जाता था । हिन्दी, हिन्दुस्तानी भाषा के नाम से आजादी के लड़ाई का मुख्य हथियार रहा । डाॅ. श्रीलाल शुक्ल ‘‘आजादी के बाद हिन्दी‘‘ में लिखते हैं -‘‘हिन्दी स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा थी । बीसवी शताब्दी के प्रारंभ में अनेक लोगो ने बचपना में हिन्दी केवल इसीलिये सीखे ताकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सके ।‘‘ मैथिलीशरण गुप्त ने खड़ी बोली में अनेक काव्या की रचना की। उनकी ‘भारत भारती‘ में स्वाधीनता आंदोलन की ललकार है। राष्ट्रीय प्रेम उनकी कविताओं का प्रमुख स्वर है। सभी बोलियों में आजादी का उदघोष है । ‘
आदिकाल से आज पर्यंत साहित्य पर बोलियों का प्रभाव बना हुआ है भक्तिकाल भक्तिपरक तो स्वतंत्रता आंदोलन में आजादी के गीत तदुपरांत समाज के विभिन्न कुरीतियों पर कटाक्ष लोकजागरण के स्वर लोकभाषा से साहित्य तक संचरित हुये हैं । आजादी के पश्चात प्रचार-तंत्र टी.वी. मीडि़या, रेडि़यो, समचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाओं के विकास के साथ-साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी हरियाणवी बोलियों में उच्चकोटि के रचनाएं गीत लोकगीत सामने आये ।
छत्तीसगढ़ी-
कोदूराम दलित‘ छत्तीसगढ़ी में कहते हैं –
अपन देश आजाद करे बर, चलो जेल संगवारी
कतको झिन मन चल देइन, आइस अब हमरो बारी ।
अवधी-
हरिश्चंद्र पांडेय ‘सरल‘ अवधी में कहते हैं-
मनई बन मनई का प्यार दे,
भेद जाति धर्म कै बिसार दे,
गंगा कै नीर गुन गाये
देसवा कै पीर गुन गाये।
हरियाणवी –
हबीब भारती की हरियाणवी रचना दृष्टव्य है-
हे दुनिया जिसनै हीणा समझै उसकी गैल पडै़ सै। हे बान बैठणा ब्याह करवाणा हे बस मैं मेरै कडै़ सै। हे ना बूज्झैं करैं सगाई, टोह कै ठोड़-ठिकाणा हे घाल जेवड़ा गेल्यां कर दें, पडै़ लाजिमी जाणा हे जिस दिन दे दें धक्का बेबे, आगै हुकम बजाणा हे यो तो बेबे घर अपणा सै, आगै देश बिराणा हे को दिन रहल्यूं मां धोरै या जितणै पार पडै़ सै
निष्कर्ष –
बोली और उपभाषा की अनेक ऐसी रचनाएं हैं, जिनके बल पर हिन्दी को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुआ । निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से हिन्दी को उनके सहगामी बोलियां समृद्ध बनाने में सदा से महत्वपूर्ण योगदान देते आ रही हैं ।
-रमेश चौहान



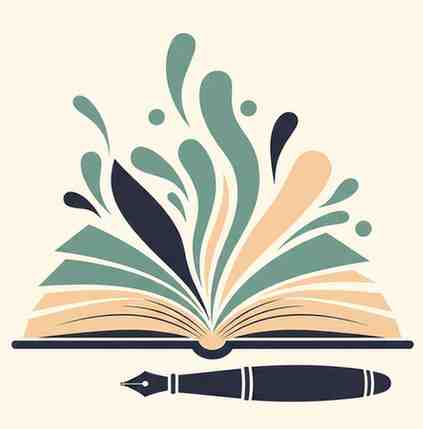

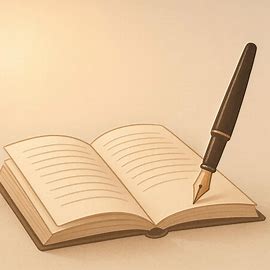
Leave a Reply