
“अस्मिता” शब्द व्यक्ति या समाज की पहचान, गौरव और आत्म-सम्मान का प्रतीक है। किसी भी समाज या क्षेत्र की अस्मिता उसके इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपरा, साहित्य, सामाजिक चेतना और राजनीतिक स्वरूप से निर्मित होती है। छत्तीसगढ़ जो मध्य भारत का हृदय कहा जाता है अपनी सांस्कृतिक धरोहर, लोकजीवन की सरलता और संसाधनों की प्रचुरता के कारण विशिष्ट पहचान रखता है।
यह भूमि न केवल प्राचीन काल से ही गौरवशाली परंपराओं की वाहक रही है बल्कि आधुनिक समय में अपनी अस्मिता की रक्षा और विकास के लिए संघर्षरत भी है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता को हम तीन आयामों में देख सकते हैं – कल (अतीत), आज (वर्तमान) और कल (भविष्य)। छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राचीन काल से समृद्ध रहा है। इसे “दक्षिण कोशल” के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक आख्यानों से लेकर पुरातात्विक साक्ष्य तक यह प्रमाणित करते हैं कि यह भूमि सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र रही। रामायण और महाभारत काल में यह क्षेत्र अपनी विशेष पहचान रखता था। रामायण में इसे माता कौशल्या की जन्मभूमि कहा गया है। बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार में भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहां अनेक बौद्ध विहारों और जैन मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। कलचुरी वंश के शासकों ने यहां शासन किया और इस क्षेत्र की कला, स्थापत्य और संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी।
छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता उसकी लोककला, लोकसंगीत, नृत्य और उत्सवों में निहित है। पंथी नृत्य, राऊत नाचा, सुआ नृत्य और करमा नृत्य इस क्षेत्र की लोक-आत्मा का प्रतीक हैं। लोकगीतों में प्रकृति, समाज और संस्कृति का सहज चित्रण होता है। गोंड, बैगा, धुरवा, माड़िया जैसी जनजातियां अपनी विशिष्ट जीवन शैली और संस्कृति के कारण छत्तीसगढ़ की अस्मिता को समृद्ध करती है। अस्मिता की रक्षा केवल सांस्कृतिक स्तर तक सीमित नहीं रही बल्कि राजनीतिक चेतना में भी दिखाई दी।
सोनाखान के वीरनारायण सिंह जिन्हें पहला शहीद कहा जाता है ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। गुंडाधुर और बस्तर के आदिवासियों ने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए विद्रोह किया। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी छत्तीसगढ़ के लोग सक्रिय रहे। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ की अस्मिता उसकी आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक गौरव और स्वतंत्रता चेतना से जुड़ी रही है। लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था बल्कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता का पुनर्जागरण था। राज्य गठन ने छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति, लोककला और संसाधनों को राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दिलाई। अब छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य अकादमी और सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी भाषा अस्मिता की धुरी है
पं. सुंदरलाल शर्मा, हरि ठाकुर , नारायण लाल परमार, श्याम लाल चतुर्वेदी,डॉ. नरेंद्र देव वर्मा, हरिहर वैष्णव,वर्मा, डुमन लाल ध्रुव आदि लेखकों ने छत्तीसगढ़ी साहित्य को ऊंचाई दी। साहित्य में अस्मिता की अभिव्यक्ति लोकगीत, कहावतों, कथाओं और आधुनिक रचनाओं में दिखाई देती है। ” अरपा पैरी के धार ” जैसे गीतों ने अस्मिता को जन-जन तक पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। नक्सलवाद अस्मिता पर सबसे बड़ी चोट है जिसने शांति और विकास को बाधित किया। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और खनन गतिविधियों ने पर्यावरण और जनजातीय जीवन को संकट में डाला। शहरीकरण और वैश्वीकरण ने पारंपरिक संस्कृति और लोकजीवन को प्रभावित किया है। चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है। धान का कटोरा कहलाने वाला यह राज्य कृषि में अग्रणी है। बस्तर दशहरा, तीजा-पोरा, छेरछेरा जैसे त्यौहार आज भी अस्मिता को जीवित रखते हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कला-संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। भविष्य में छत्तीसगढ़ की अस्मिता तभी सुरक्षित रहेगी जब लोकसंस्कृति, बोली-भाषा और परंपराओं को सहेजा जाएगा। लोककला और हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान दिलाई जानी चाहिए।छत्तीसगढ़ी भाषा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यापक स्थान देना आवश्यक है। आर्थिक विकास आवश्यक है किंतु वह जल-जंगल-जमीन की रक्षा और स्थानीय अस्मिता के साथ संतुलित होना चाहिए। खनिज संपदा का उपयोग स्थानीय लोगों के हित में होना चाहिए। सतत विकास के मॉडल को अपनाकर ही अस्मिता को सुरक्षित रखा जा सकता है। भविष्य की अस्मिता युवा पीढ़ी पर निर्भर है। उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए लोक इतिहास और संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है।
डिजिटल युग में छत्तीसगढ़ी साहित्य और संस्कृति को नए माध्यमों के जरिए विश्व पटल पर पहुंचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता तब और मजबूत होगी जब समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज को बराबरी का स्थान मिलेगा। जनजातीय अस्मिता को संरक्षित करना राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। महिला अस्मिता को आर्थिक और सामाजिक अवसर देकर मजबूती दी जा सकती है।
श्रीमती कामिनी कौशिक
रिसाईपारा धमतरी



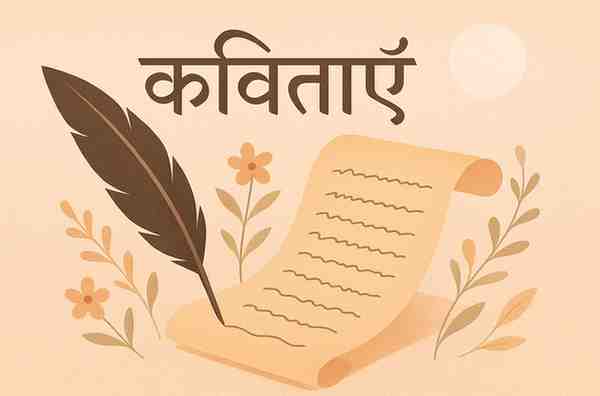

Leave a Reply